Growel Agrovet Private Limited specialises in developing, manufacturing, exporting, and marketing premium quality animal healthcare products and veterinary medicines for livestock and poultry. Our product range is designed to ensure the optimum healt...
- +91-808479239
- info@growelagrovet.com
- 51 , 5TH, A Cross, First Main Road Attur Extension, Yelahanka, Bengaluru, Karnataka, India. 560064
© 2020 Growel Agrovet Private Limited. All Rights Reserved
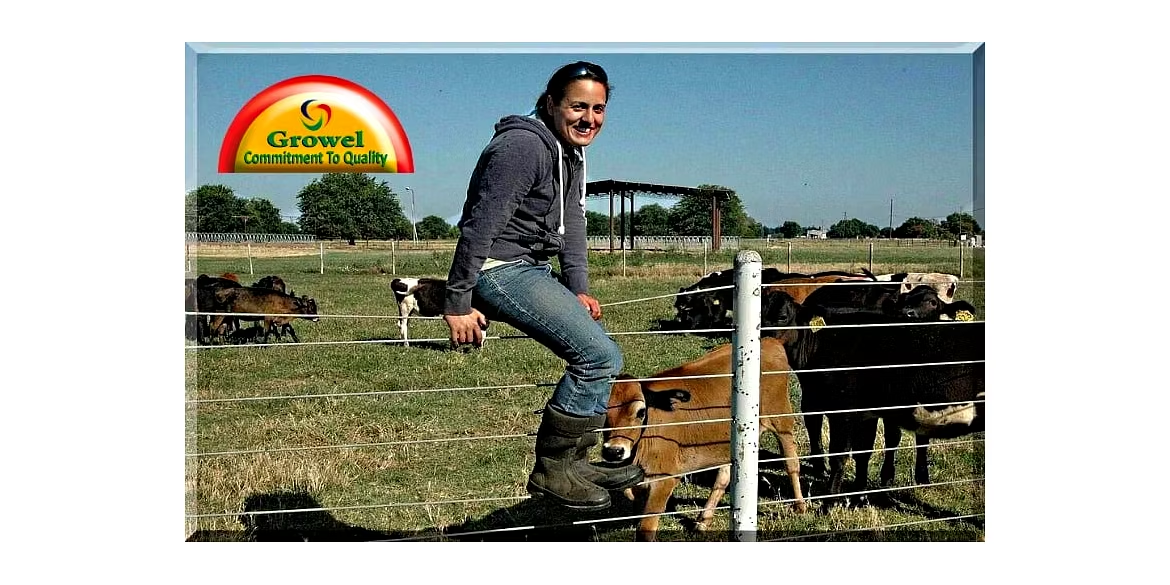
November 7, 2015
ग्रोवेल द्वारा प्रस्तुत हिंदी में पशुपालन गाइड में पशुपालन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी दी गई है ।हिंदी पशुपालन गाइड में निम्नांकित बिन्दुओं पर बिस्तृत जानकारी दी गई है । इस लेख को दो भागो में प्रकाशित किया गया है ,यह लेख हिंदी में पशुपालन गाइड का भाग दो है ।
-
पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान
-
पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ व सीमायें
-
पशुओं का बधियाकरण
-
मादा पशुओं के प्रमुख प्रजनन विकार
-
दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनका उपचार
-
पशुओं के चारे का भंडारण
पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान:
कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। भारत वर्ष में सन् 1937 में पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम प्रयोग किया गया था। आज सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा विश्व में पालतू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनायी जा रही है।
पशुओं के वीर्य का एकत्रीकरण व उसका संरक्षण:
चूने हुए अच्छे नस्ल के सांड से कृत्रिम विधि द्वारा वीर्य एकत्रित किया जाता है। सांडों को इस कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वह दूसरे अन्य नर पशु अथवा डमी (कृत्रिम पशु) पर चढ़ कर कृत्रिम योनि में वीर्य छोड़ देता है।इस एकत्रित किये वीर्य का स्थूल व सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है , स्थूल परीक्षण में वीर्य के रंग, आयतन तथा गाढापन(सघनता) का बारीकी के साथ परीक्षण किया जाता है।सूक्ष्म परीक्षण में वीर्य को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर देखा जाता है। इसमें हम वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या, उनकी गति,उनमें जीवित व मृतकों का अनुपात तथा उनमें किसी भी प्रकार की विकृति का पता लगता हैं।आज कल कई केन्द्रों पर वीर्य के कुछ विशेष परीक्षणों की भी व्यवस्था है जिससे शुक्राणुओं के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता का पता चल जाता है।वीर्य के उपरोक्त परीक्षणों के बाद कुछ विशेष माध्यमों के द्वारा उसके आयतन में वृद्धि की जाती है और फिर इस वीर्य को भविष्य में किसी भी स्थान एवं समय पर प्रयोग करने के लिये संरक्षित कर लिया जाता है।
पहले वीर्य द्रव अवस्था में ही संक्षित किया जाता था तथा इसका प्रयोग 3-4 दिन के अंदर करना पड़ता था क्योंकि उसके बाद उसकी गुणवत्ता में काफी कमी आ जाती थी।लेकिन आजकल वीर्य को तरल नत्रजन के अंदर जमी हुई अवस्था में रखा जाता है।घन हिमीकृत वीर्य को वर्षों तक तरल नत्रजन में बिना गुणवत्ता को प्रभावित किये हुये रहता है। हिमीकृत वीर्य को एक स्थान से दूसरे सतह तक तरल नत्रजन के अंदर आसानी से ले जाया जा सकता है।इस प्रकार एक देश से दूसरे देश को भी उन्नत श्रेणी के सांड का वीर्य सुविधापूर्वक भेजा जा सकता है।
गहन हिम्कृत वीर्य द्वारा पशुओं में गर्भाधान की विधि:
आजकल सम्पूर्ण विश्व में ज्यादातर गहन हिम्कृत वीर्य का ही प्रयोग होने लगा है।इसमें एक प्रशिक्षित व्यक्ति हिम्कृत वीर्य को पुन: द्रव अवस्था में लाकर कृत्रिम गर्भाधान गन की सहायता से रेक्टोविजायनल विधि द्वारा गर्मायी हुई मादा की प्रजनन नली में डालता है।
वीर्य का द्रवीकरण (थाइंग करना):
हिम्कृत वीर्य को प्रयोग करने से पहले इसे सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में लाया जाता है। इस क्रिया को थाइंग कहते हैं।इसमें एक बीकर में 37 डि०से० तापमान पर पानी लिया जाता है। हिम्कृत वीर्य के तृण को तरल नत्रजन कन्टेनर से निकल कर बीकर में रखे पानी में 15 से 30 सेकिंड के लिये रखते हैं। इसके बाद तृण को पानी से निकाल कर उसे सुखा लिया जाता है।
वीर्य तृण को कृत्रिम गर्भाधान गन में भरना:
कृत्रिम गर्भाधान गन एक 18-19 इंच लम्बी धातु की नली होती है जिसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है।इसके एक सिरे पर प्लास्टिक का एक छल्ला होता है।थाइंग के पश्चात वीर्य तृण का फैक्टरी प्लग वाला सिरा गन के अंदर रखा जाता है तथा पोलिविनायल से सिल किये सिरे को गन से बाहर रखते हैं।इसके पश्चात गन से बाहर वाले सिरे को एक साफ कैँची अथवा स्ट्रा कटर की सहायता से समकोण पर काट देते हैं और एक प्लास्टिक की शीथ को कृत्रिम गर्भाधान गन के ऊपर चढ़ाते हैं जिसे छल्ले के द्वारा अपने स्थान पर ठीक से कस दिया जाता है।अब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर की ओर दबा कर वीर्य तृण से वीर्य के बचाव को चैक किया जाता है।
पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की विधि:
आरंभ में कृत्रिम गर्भाधान विजाइनल विधि द्वारा किया जाता था जिसमें वीर्य को विजाइनल स्पैकुलम की सहायता से कृत्रिम गर्भाधान केथेटर द्वारा पशु की गर्भाशय ग्रीवा में रखा जाता था।लेकिन अब पूरे विश्व में रेकटो विजाइनल विधि द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है।इस विधि में कृत्रिम गर्भाधान तक्नीशियन अपने बायें हाथ को साबुन-पायी या तेल आदि से चिकना करके उसे कृत्रिम गर्भाधान के लिये आए पशु की गुदा में डालता है और गर्भाशय ग्रीवा को हाथ में पकड़ लेता है।तत्पश्चात वह दूसरे हाथ में कृत्रिम गर्भाधान गन को योनि में प्रविष्ट करते हुए उसे ग्रीवा तक पहुंचता है तथा गुदा में स्थित हाथ के अंगूठे की सहायता से गन को ग्रीवा के बाहरी द्वार में प्रविष्ट करा देता है। इसके पश्चात ग्रीवा की सम्पूर्ण लम्बाई को पार करते हुए गन के सिरे को गर्भाशय बाडी में पहुंचाया जाता है। फिर दाहिने हाथ से पिस्टल दबाकर गन में भरे वीर्य को वहां छोड़ दिया जाता है।
विजाइनल स्पैकुलम विधि की तुलना में रेक्टोविजाइनल विधि के निम्न लिखित प्रमुख लाभ हैं:
(1) गुदा में हाथ डाल कर पशु के प्रजनन अंगों का भली प्रकार परीक्षण किया जा सकता है तथा उसकी गर्मी का सही पता लग जाता है।
(2) अनेक बार गर्भ धारण किए पशु भी गर्मीं में आ जाते हैं और उन्हें अज्ञानता में गर्भाधान के लिए ले जाया जाता है| ऐसे पशु का इस विधि द्वरा गर्भ परीक्षण भी हो जाता है और वह व्यर्थ में दोबारा गर्भाधान करके गर्भपात के खतरे से बच जाता है।
(3) इस विधि में वीर्य को उचित स्थान पर छोड़ा जाता है जिससे वीर्य व्यर्थ में बर्बाद नहीं होता तथा इसमें गर्भधारण की संभावना अधिक होती है।
पशुओं के गर्भाधान का उचित समय व सावधानियाँ:
पशु के मद काल का द्वितीय अर्धभाग कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त होता है।पशु पालक को पशु को गर्भधारण के लिए लाते व ले जाते समय उसे डराना या मारना नहीं चाहिए क्योंकि इसे गर्भ धारण किये हुये अधिकांश पशुओं में मद च्रक शुरू हो जाता है, लेकिन ब्याने के 50-60 दिनों के बाद ही पशु में गर्भाधान करना उचित रहता है क्योंकि उस समय तक ही पशु का गर्भाशय पूर्णत: सामान्य अवस्था में आ पाता है।प्रसव के 2-3 माह के अंदर पशु को गर्भ धारण कर लेना चाहिए ताकि 12 महीनों के बाद गाय तथा 14 महीनों के बाद भैंस दोबारा बच्चा देने में सक्षम हो सके क्योंकि यही सिद्धांत दुधारू पशु पालन में सफलता की कुंजी है।
पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लाभ व सीमायें:
प्राकृतिक गर्भाधान की तुलना में कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ हैं जिनमें प्रमुख लाभ निम्नलिखित है:-
(1) कृत्रिम गर्भाधान तकनीक द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाले सांड को अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है।प्राकृतिक विधि में एक सांड द्वारा एक वर्ष में 50-60 गाय या भैंस को गर्भित किया जा सकता है जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से एक वर्ष में हजारों की संख्या में गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है।
(2) इस विधि में धन एवं श्रम की बचत होती हसी क्योंकि पशुपालक को सांड पालने की आवश्यकता नहीं होती।
(3) कृत्रिम गर्भाधान में बहुत दूर यहां तक कि विदेशों में रखे उत्तम नस्ल व गुणों वाले सांड के वीर्य को भी गाय व भैंसों में प्रयोग करके लाभ उठाया जा सकता है।
(4) अत्तिउत्तम नस्ल के सांड के वीर्य को उसकी मृत्यु के बाद भी प्रयोग किया जा सकता है।
(5) इस विधि में उत्तम गुणों वाले बूढ़े या घायल सांड का प्रयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है।
(6) कृत्रिम गर्भाधान में सांड के आकार या भर का मादा के गर्भाधान के समय कोई फर्क नहीं पड़ता।
(7) इस विधि में विकलांग गायों-भैंसों का प्रयोग भी प्रजनन के लिए किया जा सकता है।
(8) कृत्रिम गर्भाधान विधि में नर से मादा तथा मादा से नर में फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है।
(9) इस विधि में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे मादा की प्रजनन की बीमारियों में काफी हद तक कमी आ जाती है तथा गर्भधारण करने की डर भी बढ़ जाती है।
(10)इस विधि में पशु का प्रजनन रिकार्ड रखने में भी आसानी होती है।
कृत्रिम गर्भाधान के अनेक लाभ होने के बावजूद इस विधि की अपनी कुछ सीमायें है जो मुख्यत: निम्न प्रकार है|
(1) कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति अथवा पशु चिकित्सक की आवश्यकता होती है तथा कृत्रिम गर्भाधान तक्नीशियन को मादा पशु प्रजनन अंगों की जानकारी होना आवश्यक है।
(2) इस विधि में विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है।
(3) इस विधि में असावधानी वरतने तथा सफाई का विशेष ध्यान रखने से गर्भ धारण की दर में कमी आ जाती है।
(4) इस विधि में यदि पूर्ण सावधानी न वरती जाये तो दूरवर्ती क्षेत्रों अथवा विदेशों से वीर्य के साथ कई संक्रमक बीमारियों के आने का भी भय रहता है।
पशुओं का बधियाकरण:
बधियाकरण के लाभ:
नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मादा के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया को बधियाकरण कहते हैं।उन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम की सफलता के लिए अवांक्षित नर पशुओं का बधियाकरण बहुत ही आवश्यक कार्य जिसके बिना डेयरी पशुओं की नस्ल में सुधार करना असम्भव हैं।बछड़ों में बधियाकरण की उचित आयु 2 से 8 माह के बीच होती हैं।
(1) बधियाकरण द्वारा निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढने से रोका जा सकता है जिससे उसके द्वारा असक्षम एवं अवांक्षित सन्तान पैदा ही नहीं होती जोकि सफल एवं लाभकारी पशुपालन के लिए आवश्यक है।
(2) बधिया किए गये नर पशु को मादा पशुओं के साथ बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है क्योंकि वह मद में आई मादा के ऊपर नहीं चढता।
(3) बधिया किए गये पशु को आसानी से नियन्त्रित किया जा सकता है।
(4) बधियाकरण से मांस के लिये प्रयोग होने वाले पशुओं के मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है।
बधियाकरण की विधियाँ:
पालतू पशुओं में बधियाकरण सबसे पुरानी शल्य क्रिया समझी जाती है।बधियाकरण निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है।
(क) शल्य क्रिया द्वारा बधियाकरण:
इस विधि में शल्य क्रिया द्वारा अंडकोषों के ऊपर चढ़ी चमड़ी (स्क्रोटम) को काटकर दोनों अंडकोषों को निकाल दिया जाता है। इस क्रिया में में पशु के एक छोटा सा घाव हो जाता है जोकि एंटीसेप्टिक दवाईयों के प्रयोग करके कुछ समय के पश्चात ठीक हो जाता है।
(ख) बर्डिजो कास्ट्रेटर द्वारा बधियाकरणल:
यह विधि आज-कल नर गोपशुओं व भेंसों में बधियाकरण के लिये सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें एक विशेष प्रकार का यंत्र जिसे बर्डिजो कास्ट्रेटर कहते हैं प्रयोग किया जाता है। इस विधि में रक्त बिल्कुल भी नहीं निकलता क्योंकि इसमें चमड़ी को कटा नहीं जाता। इसमें पशु के अंड कोशों से ऊपर की और जुडी स्पर्मेटिक कोर्ड जिकी चमड़ी के नीचे स्थित होती है, को इस यन्त्र के द्वारा बाहर से दबा कर कुचल दिया जाता है जिससे अंडकोषों में खून का दौरा बन्द हो जाता है।फलस्वरूप अंडकोष स्वत:ही सुख जाते हैं।
बर्डिजो कास्ट्रेटर द्वारा बधियाकरण करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतना आवश्यक है :
(1)बर्डिजो कास्ट्रेटर को दबाते समय स्पर्मेटिक कोड स्लिप नहीं करनी चाहिए।
(2)कास्ट्रेटर में अंडकोष नहीं दबाना चाहिये अन्यथा अंडकोषों में भारी सूजन आ जाती है जिससे पशु को तकलीफ होती है।
(3)कास्ट्रेटर में चमड़ी का फोल्ड नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे चमड़ी के नीचे घाव होने का खतरा रहता है।
(4)कास्ट्रेटर को प्रयोग करने से पहले ठीक प्रकार से साफ कर लेना चाहिए।
(ग) रबड़ के छल्ले द्वारा बधियाकरण:
पश्चिमी देशों में प्रचलित यह विधि बहुत छोटी उम्र के बछड़ों में प्रयोग की जाती है। इसमें रबड़ का एक मजबूत व लचीला छल्ला अंड कोषों के ऊपरी भाग स्थित स्परमेतिक कोर्ड के ऊपर चढा दिया जाता है जीके दबाव से अंडकोषों में खून का दौरा बन्द हो जाता है। इससे अंडकोष सुख जाते हैं तथा रबड़ का छल्ला अंडकोषों से निकल कर नीचे गिर जाता है।
मादा पशुओं के प्रमुख प्रजनन विकार :
(क) रिपीट ब्रिडिंग(पशु का बार-बार गर्मीं में आना) :
प्रजनन का यह विकार पशु पालकों तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पशु पालकों को पशु के गर्भ धारणण कर पाने के कारण बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है। इसमें पशु दो या दो से अधिक बार गर्भाधान करने के बावजूद गर्भधारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित मदचक्र में बना रहता है। सामान्य परीक्षण के दौरान वह लगभग नि:रोग लगता है।रिपीट ब्रिडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें से निम्नलिखित कारण प्रमुख है:-
(ख) पशु की प्रजनन नली में वंशानुगत, जन्म से अथवा जन्म के बाद होने वाले विकार :
इनमें प्रजनन नली के अंगों में किसी एक खंड का ण होना, अंडाशय का बरसा के साथ जुड जाना, अंडाशय में रसौली, गर्भाशय ग्रीवा का टेढ़ा होना(kinked cervix), डिम्ब वाहनियों में अवरोध का होना, गर्भाशय की अंदर की परत (endometrium) में विकार आदि शामिल है।
(ग) शुक्राणुओं, अंडाणु तथा प्रारम्भिक भूर्ण में वंशानुगत, जन्म जात तथा जन्म के बाद होने वाले विकार :
इनमें काफी देर से अथवा मदकल के समाप्त होने पर गर्भाधान कराने के कारण अंडाणु का निषेचन योग्य समय निकल जाना, अंडाणु अथवा शुक्राणु में विकार,एक ही सांड के वीर्य का कई पीडियों में प्रयोग (breeding), शुक्राणु व अंडाणु में मेल न होना, मद काल की प्रारम्भिक अवस्था (early heat) में गर्भाधान कराना जिससे अंडाणु के पहुंचने तक शुक्राणु पुराने हो जाते हैं, आदि प्रमुख हैं।
(घ) पशु प्रबंध में कमियाँ :
इनमें पशुपालक द्वारा पशु के मद काल में होने का सही पता न लगा पाना, अकुशल व्यक्ति से कृत्रिम गर्भाधान करना, पशु के कुपोषण तथा पशु में तनाव (strees) इत्यादि शामिल है।पशु कुपोषण के कभी शिकार ना हों ,इसके लिए आप उन्हें विश्वप्रसिद्ध मिनरल मिक्चर Chelated Growmin Forte (चिलेटेड ग्रोमिन फोर्ट) और Immune Booster Premix (इम्यून बुस्टर प्री-मिक्स) नियमित रूप से दें।
(ड.) अंत: स्रावी विकार :
इनमें अंडाणु का अंडाशय से बाहर न आना (anovulation), फोलिकल का समय हो जाना (follicilar atressia) अंडाणु का अंडाशय से बाहर आना (delayed ovulation), सिस्टिकओवरी, कोरपस ल्युटियम का असक्षम होना (luteal insufficienc),(weak heat) आदि शामिल है।
(च) प्रजनन अंगों के संक्रामक रोग अथवा उनकी सूजन :
इन् रोगों में ट्रायकोमोनास फीटस, विब्रियो फीटस, ब्रुसेलोसिस, आई.बी.आर-आई.पी.वी. कोरिनीबैक्टेरियम पायोजनीज तथा अन्य जीवाणु व विषाणु शामिल है।इसमें गर्भाशय में सूजन हो जाती है जिससे भ्रूण की प्रारम्भिक अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है।
उपचार व निवारण :
(1) रिपीट ब्रीडर पशु का परीक्षण व उपचार पशु चिकित्सक से करना चाहिए से करना चाहिए ताकि इसके कारण का सही पता लग सके।ऐसे पशु को कई बार परीक्षण के लिये बुलाना पड़ सकता है क्योंकि एक बार पशु को देखने से पशु चिकित्सक का किसी खास नतीजे पर पहुंचना कठिन होता है।अंडाशय से अंडाणु निकलता है या नहीं इसका पता पशु का मद काल में तथा मद काल में तथा के 10 दिन के बाद पुन: परीक्षण करके लगाया जा सकता है।दस दिन के बाद परीक्षण करने पर पशु की और भी बहुत सी बीमारियों का पता पशु चिकित्सक लगा सकते हैं। अत: पशु चिकित्सक की सलाह पर पशुओं को उसके परीक्षण तथा इलाज के लिये अवश्य लाना चाहिये।
(2) डिम्ब वाहनियों में अवरोध जोकि रिपीटब्रीडिंग का एक मुख्य कारण है का पता एक विशेष तकनीक जिसे मोडिफाइड पी एस पी टेस्ट कहते हैं, द्वारा लगाया जा सकता हैं।अत: स्रावी विकार के लिए कुछ विशेष हारमोन्स जी.एं.आर.एच.अथवा एल.एच.आदि लगाए जाते हैं।
(3) मद काल में पशु के गर्भाशय से म्यूकस एकत्रित कर सी.एस.ति. परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है जिससे गर्भाशय के अंदर रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं का पता लग जाता हैं तथा उन पर असर करने वाली दवा भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार उस दवा के प्र्यिग से गर्भाशय के संक्रमण को नियन्त्रित किया जा सकता है।
(4) पशु के मद काल का पशु पालक को विशेष ध्यान रखना चाहिए इसके किए उसे पशु में मद के लक्षणों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। ताकि वह पशु का मद की सही अवस्था (द्वितीय अर्ध भाग) में गर्भाधान करा सके।
(5) पशु पालक को पशु के सही मद अवस्था में न होने की दिशा में उसका जबरदस्ती गर्भाधान नहीं करना चाहिए तथा कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को भी अनावश्यक रूप से पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे रिपीटब्रीडर की संख्या बढ़ती है और पशु को कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।
(6) रिपीटब्रीडर पशु को गर्भाशय ग्रीवा के मध्य में गर्भाधान करना उचित है क्योंकि कुछ पशुओं में गर्भधारण के बाद भी मदचक्र जारी रहता है। ऐसे पशु का गर्भाशय के अंदर गर्भाधान करने से भ्रूण की मृत्यु की मृत्यु की पूरी सम्बह्वना रहती है।
(7) पशु पालक को पशु की खुराक पर विशेष ध्यान देना चाहिए।कुपोषण के शिकार पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पशु में खनिज मिश्रण व विटामिन्स ई आदि की कमी से प्रजनन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पशुओं को नियमित रूप से Chelated Growmin Forte (चिलेटेड ग्रोमिन फोर्ट) , Immune Booster Premix (इम्यून बुस्टर प्री-मिक्स) और Grow E-Sel (ग्रो ई-सेल) देनी चाहिए।
(8)देर से अंडा छोड़ने वाले पशु (delayed ovulator) में 24 घंटे के अंतराल पर 2-3 बार गर्भाधान कराने से अच्छे परीक्षण मिलते है।
(2)पशु का मद में न आना:
यौवनावस्था प्राप्त करने के बाद मादा पशु में मद चक्र आरंभ हो जाता है तथा यह चक्र सामान्यत: तब तक चलता रहता है जब तक कि वह बूढा होकर प्रजनन में असक्षम नहीं हो जाता। प्रजनन अवस्था में यदि पशु मद में नहीं आता तो इस स्थिति को एनस्ट्रस को टू अनस्ट्रस भी कहते हैं।यह निम्नलिखित द्वितीय श्रेणी एनस्ट्रस।
प्रथम श्रेणी एनस्ट्रस:
इस श्रेणी के एनस्ट्रस में अंडाशय के ऊपर मद चक्र की कोई रचना जैसे फोलीकल अथवा कोरपस ल्यूटियम नहीं पायी जाती।इस एनस्ट्रस को ट्रू अनस्ट्रस भी कहते है। यह निम्नलिखित कारणों से हो सकता है।
(क) कुपोषण (ख) वृद्धावस्था (ग) अत: व बह्मा परजीवी तथा लम्बी (chronic) बीमारियां (घ) ऋतु का प्रभाव (विशेष कर भैंसों में) (ड़) प्रजनन अंगों के विकार|
द्वितीय श्रेणी एनस्ट्रस:
इस वर्ग के एनस्ट्रस में एनस्ट्रस में अंडाशय के ऊपर मद चक्र की रचना जैसे कार्पस ल्यूटियम अथवा फोली कल आदि पाई जाती है| यह एनस्ट्रस निम्नलिखित कारणों से हो सकता है।
(क)गर्भावस्था:
गर्भ धारण के पश्चात कोर्पस ल्युटियम प्रोजेस्टरोन हार्मोन का स्राव करने लगती है।यह हार्मोन पशु को गर्मीं में आने से रोकता है| अत: गर्भावस्था पशु के मद में न आने का प्रमुख कारण हैं।
(ख)दृढ कोर्पस ल्युटियम (persistent corpus luteum) के कारण एनस्ट्रस : इस अवस्था में गर्भाशय में पीक पड़ जाने अथवा अन्य किसी कारण से अंडाशय में कार्पस ल्युटियम खत्म न होकर क्रियाशील अवस्था में बनी रहती है जोकि पशु को गर्मीं में आने से रोकती है।
(ग)ल्युटियल सिस्ट के कारण एनस्ट्रस:
इसमें अंडाशय में एक सिस्ट बन जाता है जिससे प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव होता है फलस्वरूप पशु गर्मीं में नहीं आता।
(घ)कमजोर मद के कारण एनस्ट्रस:
इसमें पशु में बाहर से गर्मीं के लक्षण दिखायी नहीं देते लेकिन पशु खामोश अवस्था में गर्मीं में आता रक्त है और नियत समय पर अंडाशय से अंडाणु भी निकलता है।
उपचार तथा निवारण:
(1) पशु को सदैव सन्तुलित आहार देना चाहिए देना चाहिए तथा पशु के आहार में खनिज मिश्रण Chelated Growmin Forte (चिलेटेड ग्रोमिन फोर्ट) और Immune Booster Premix (इम्यून बुस्टर प्री-मिक्स) अवश्य मिलाना चाहिए।
(2) पशु के मद में न आने पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
(3) आवश्यकतानुसार पशु को पेट के कीड़ों की दवा भी अवश्य देनी चाहिए।
(4) यदि पशु स्थिर कोर्पस ल्युटियम अथवा ल्युटियल सिस्ट के कारण गर्मीं में नहीं आता तो उसे प्रोस्टाग्लेंडीन का टीका लगाया जाता है।
(5) गोनेडोट्रोफिन्स,जी.एं.आर.एच.,विटामिन ए तथा फोस्फोरस के टीके भी एनस्ट्रस में दिए जाते हैं लिकिन ये पशु चिकित्सक द्वारा ही लगाए जाने चाहिए।
(7)गर्भाशय ग्रीवा पर ल्युगोल्स आयोडीन का पेंट करने से भी इस विकार में लाभ होता हैं।
मेट्राइटिस/एन्डोमेट्राइटिस (गर्भाशय शोथ):
मेट्राइटिस अथवा गर्भाशय शोथ का अर्थ है सम्पूर्ण गर्भाशय में सूजन होना तथा एन्डोमेट्राइटिस गर्भाशय के अंदर की पर्त की सूजन को कहते हैं।अधिकांशत:इसमें ओशु का सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहता है लेकिन उसकी प्रजन क्षमता पर इसका कुप्रभाव पड़ता है।मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस पशुओं में कुछ विशेष बीमारियों के बाद उत्पन्न होती है जैसे कि कष्ट प्रसव, ब्याने के बाद साल (प्लेसेंटा) का रुक जाना तथा कुछ अन्य कारण। प्रसव के समय कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्रा०ग० के समय पर फिर सीधे रक्त परिवहन से रोगाणु गर्भाशय में प्रवेश करके मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस पैदा कर सकते हैं।कई अन्य बीमारियां जैसे कि ब्रुसिलोसिस, ट्राइकोमोनिओसिस तथा विब्रियोसिस आदि भी एन्डोमेट्राइटिस पैदा करके पशु में बाँझपन पैदा कर सकती है।
मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस का प्रमुख लक्षण योनि से सफेद-पीले रंग का गर्व पदार्थ बाहर निकलना है।इसकी मात्रा बीमारी की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा सबक्लीनिकल एन्डोमेट्राइटिस के केसों में इस प्रकार का कोई पदार्थ निकलता दिखायी नहीं देता।
उपचार व रोकथाम:
मेट्राइटिस अथवा एन्डोमेट्राइटिस का उपचार गर्भाशय में उपयुक्त दवा जैसे एंटीबायोटिक आदि डालकर किया जाता है।इसके अतिरिक्त एंटीबायोटिक के टीके मांस भी में लगाए जा सकते है।गर्भाशय से एकत्रित पदार्थ का सी.एस.टी.करवा के उपयुक्त औषधि का प्रयोग इस बीमारी का सर्वोत्तम उपचार है।पशु के ब्याने के समय तथा कृत्रिम अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के समय सफाई का पूरा ध्यान रखकर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है।
(4)पायोमेट्रा (गर्भाशय में पीक पड़ जाना):
पायोमेट्रा में पशु के गर्भाशय में पीक इकट्ठी हो जाती है।इसमें पशु गर्मी में नहीं आता तथा समय-समय पर उसकी योनि से सफेद रंग का डिस्चार्ज निकलता देखा जा सकता है। पशु का परीक्षण करने पर उसकी योनि में सफेद रंग का द्रव पदार्थ दिखता है गुदा द्वारा परीक्षा करने पर गर्भाशय फूली हुई अवस्था में पाया जाता है।अधिकांशत: पशु के अंडाशय में कोर्पस ल्युटियम भी पायी जाती है। इस बीमारी का पशु की गर्भावस्था से अंतर करना आवश्यक ओता है क्योंकि कई बार ऐसे मादा पशु को गलती सेगर्भवती समझ लिया जाता है।
उपचार:
इस बीमारी का सबसे अच्छा व आधुनिक इलाज प्रोस्टाग्लेंड़िन एफ-2 अल्फ़ा का इंजेक्शन देना है।इस टीके के प्रयोग से सी.एल.खत्म ही जाती है जिससे पशु मद में आ जाता है और गर्भाशय में भरा सारा पीक बाहर निकल जाता है।
(5)गर्भपात:
गाय व भैंसों में गर्भपातवह वह अवस्था है जिससे कृत्रिम अथवा प्राकृतिक गर्भाधान के द्वारा गर्भ धारण किए पशु अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सामान्य गर्भावस्था पूरी होने के लगभग 20 दिन पहले तक की अवधि में किसी भी समय गर्भाशय से बाहर फेंक देता है। यह बच्चा या तो मर हुआ होता है या फिर वह 24 घण्टों से कम समय तक ही जीता है।प्रारम्भिक अवस्था में (2-3 माह की अवधि तक)होने वाले गर्भपात का पशु पालकों को कई बार पता ही नहीं चलता तथा पशु जब पुन: गर्मी में आता है तो वे उसे खाली समय बैठते है| डो या तीन माह के बाद गर्भपात होने पर पशु पालकों को इसका पता लग जाता है।
(6)गर्भपात के कारण:
गाय या भैंसों में गर्भपात होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं।
(क)संक्रामक कारण:
इनमें जीवाणुओं के प्रवेश द्वारा पैदा होने वाली बीमारियां ट्रायकोमोनिएसिस,विब्रियोसिस, ब्रूसेल्लोसिस, साल्मोनेल्लोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, फफूंदी तथा अनेक वाइरल बीमारियां शामिल है।
उपचार व रोकथाम:
यदि पशु में गर्भपात के लक्षण शुरू हो गए हो तो उस में इसे रिक पाना कठिन होता है।अत: पशु पालकों को उन कारणों से दूर रहना चाहिए जिनसे गर्भपात होने की सम्भावना होती है।गर्भपात की रोक थम के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1. गौशाला सदैव साफ सुथरी रखन चाहिए तथा उसमें बीच-बीच में कीटाणु नाशक दवा Viraclean (विराक्लीन) का नियमित रूपसे छिड़काव करना चाहिये।पशुशाला एवं पशुओं के नाद और बाल्टी इत्यादि को नियमित रूप से Viraclean (विराक्लीन) से धोना चाहिये।
2. गाभिन पशु की देखभाल का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा उसे चिकने फर्श पर नहीं बांधना चाहिए।
3. गाभिन पशु की खुराक का पूरा ध्यान रखना चाहिए तथा उसे सन्तुलित आहार देना चाहिए।
4. मद में आए पशु का सदैव प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन द्वारा ही गर्भधान करना चाहिए।
5. गर्भपात की सम्भावना होने पर शीघ्र पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
6. यदि किसी पशु में गर्भ पात हो गया हो तो उसकी सुचना नजदीकी पशु चिकित्सालय में देनी चाहिए ताकि इसके कारण का सही पता चल सके।गिरे हुए बच्चे तथा जेर को गड्ढे में दबा देना चाहिए तथा गौशाला को ठीक प्रकार से किटाणु नाशक दवा Viraclean (विराक्लीन) से साफ करना चाहिए।
(6)ब्याने के बाद जेर का न निकलना:
गाय व भैंसों में ब्याने के बाद जेर का बाहर न निकलना अन्य पशुओं की अपेक्षा काफी ज्यादा पाया जाता है।सामान्यत:ब्याने के 3से 8 घंटे के बीच जेर बाहर निकल जाती है।लेकिन कई बार 8 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी जेर बाहर नहीं निकलती।कभी कभी यह भी देखा गया है कि आधी जेर टूट कर निकल जाती है तथा आधी गर्भाशय में हे रह जाती है।
कारण :-जेर न निकलने के अनेक कारण हो सकते हैं।संक्रामक करणों में विब्रियोसिस, , लेप्टोस्पाइरोसिस,टी.बी., फफूंदी,विरस तथा कई अन्य वाइरस तथा कई अन्य संक्रमण शामिल है लेकिन ब्रूसेल्लोसिस बीमारी में जेर न निकलने की डर सबसे अधिक होती है।असंक्रामक कारणों में असंक्रामक गर्भपात, समय से पहले प्रसव, जुड़वाँ बच्चे होना, कष्ट प्रसव, वृधाब्यानेव्स्था के बाद पसु को बहुत जल्दी गर्भित कराना, कुपोषण,हार्मोन्स का असंतुलन आदि प्रमुख है।
लक्षण:- गर्भाशय में जेर के रह अंदर सड़ने लगती है तथा योनि द्वार से बदबूदार लाल रंग का डिस्चार्जनिकलने लगता है।पशु की भूख कम हो जाती है तथा दूध का उत्पादन भिगिर जाता है।कभी कभी उसे बुखार भी हो जाता है।गर्भाशय में संक्रमण के कारण पशु स्ट्रेनिंग(गर्भाशय को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है जिससे योनि अथवा गर्भाशय तथा कई बार गुदा भी बाहर निकल आते है तथा बीमारी जटिल रूप ले लेती है।
उपचार व रोकथाम:
पशु की जेर को हाथ से निकालने के समय के बारे में विशेषज्ञों के अलग-अलग मत है।कई लोग ब्याने के 12 घंटे के बाद जेर से निकालने की सलाह देते हैं जबकि अन्य 72 घण्टों तक प्रतीक्षा करने के बाद जेर हाथ से निकलवाने की राय देते हैं।यदि जेर गर्भाशय में ढीली अवस्था में पड़ी है तो उसे हाथ द्वारा बाहर निकलने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन यदि जेर गर्भाशय से मजबूती से जुडी है तो इसे जबरदस्ती निकालने से रक्त स्राव होने तथा अन्य जटिल समस्यायें पैदा होने की पूरी सम्भावना रहती है।ब्याने के बाद ओक्सीटोसीन अथवा प्रोस्टाग्लेंड़िन एफ-2 एल्फा टीकों को लगाने से अधिकतर पशु जेर आसानी से गिरा देते हैं।लेकिन ये टीके पशु चिकित्सक की सलाह से ही लगवाने चाहिए।पशु की जेर हाथ से निकलने के बाद गर्भाशय में जीवाणु नाशक औषधि अवश्य रखनी चाहिए तथा उसे दवाइयां देने का कं पशु चिकित्सक से ही करवाना चाहिए, पशु पालक को स्वयं अथवा किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से यह कार्य नहीं करवाना चाहिए। पशु को गर्भावस्था में खनिज मिश्रण तथा सन्तुलित आहार अवश्य देना चाहिए। प्रसव से कुछ दिनों पहले पशु को विटामिन ई का टीका लगवाने से यह रोग किया जा सकता है।
(7) गर्भाशय का बाहर आजाना (प्रोलैप्स ऑफ यूटरस):
कई बार गाय व भैंसों में प्रसव के 4-6 घंटे के अंदर गर्भाशय बाहर निकल आता है जिसका उचित समय पर उपचार न होने पर स्थिति उत्पन्न हो जाती है।कष्ट प्रसव के बाद गर्भाशय के बाहर निकलने की संभावना अधिक रहती है।इसमें गर्भाशय उल्टा होकर योनि से बाहर आ जाता हैं तथा पशु इसमें प्राय: बैठ जाता है।गर्भाशय तथा अंदर के अन्य अंगों को बाहर निकलने की कोशिश में पशु जोर लगाता रहता है जिससे कई बार गुददा भी बहार आ जाता है तथा स्थिति और गम्भीर हो जाती है।
गर्भाशय के बाहर निकलने के मुख्य कारण निम्नलिखित है:-
(क) पशु की वृद्धावस्था
(ख) कैलसियम की कमी
(ग) कष्ट प्रसव जिसके उपचार के लिए बच्चे को खींचना पड़ता है
(घ) प्रसव से पूर्व योनि का बाहर आना
(ड़) जेर का गर्भाशय से बाहर न निकलना
उपचार व रोकथाम:
जैसे ही पशु में गर्भाशय के बाहर निकलने का पता चले उसे दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए ताकि बाहर निकले अंग को दूसरे पशुओं से नुक्सान न हबाहर निकले अंग को गीले तौलिए अथवा चादर से ढक देना चाहिए तथा यदि संभव हो तो बाहर नीले अंग को योनि के लेवल से थोड़ा ऊँचा रखना चाहिए ताकि बाहर निकले अंग में खून इकट्ठा न हो। बाहर निकले अंग को अप्रशिक्षित व्यक्ति से अंदर नहीं करवाना चाहिए बल्कि उपचार हेतू शीघ्रातिशीघ्र पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए।यदि पशु में कैल्शियम की कमी है तो पॉवरफुल कैल्शियम टॉनिक Grow-Cal D 3 ( ग्रो-कैल डी3) सुबह और शाम में नियमित रूप से दिया जाता है।बाहर निकले अंग को कोसे गर्म पानी अथवा सेलाइनके पानी से ठीक प्रकार साफ कर लिया जाता है।यदि ग्र्भाह्य के साथ जेर भी लगी हुई है टो उसे जबरदस्ती निकलने की आवश्यकता नहीं होती।हथेली के साथ सावधानी पूर्वक गर्भाशय को अंदर किया जाता है तथा उसे अपने स्थान पर रखने के उपरांत योनि द्वार में टांके लगा दिए जाते हैं।इस बीमारी में यदि पशु का ठीक प्रकार से इलाज न करवाया जाए टो पशु स्थायी बांझपन का शिकार हो सकता है।अत: पशु पालक को इस बारे में कभी ढील नहीं बरतनी चाहिए।गर्भावस्था में पशु की उचित देख भाल करने तथा उसे अच्छे किस्म के खनिज मिश्रण से साथ सन्तुलित आहार देने से इस बीमारी की सम्भावना को कम किया जा सकता है।पशुओं को कैल्शियम टॉनिक Grow-Cal D 3( ग्रो-कैल डी3) तथा विटामिन ई व सेलेनियम Grow E-Sel (ग्रो ई-सेल) देने से भी लाभ हो सकता है।
दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनका उपचार:
दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियाँ होती है।सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, अंत: व ब्रह्मा परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण तथा शरीर के अंदर की चयापचय (मेटाबोलिज्म) क्रिया में विकार आदि प्रमुख कारणों में है। इन बीमारियों में बहुत सी जानलेवा बीमारियां है था कई बीमारियाँ पशु के उत्पादन पर कुप्रभाव डालती है।कुछ बीमारियाँ एक पशु से दूसरे पशु को लग जाती हैजैसे मुह व खुर की बीमारी, गल घोंटू, आदि, छूतदार रोग कहते हैं। कुछ बीमारियाँ पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती है जैसे रेबीज़ (हल्क जाना), क्षय रोग आदि, इन्हें जुनोटिक रोग कहते हैं| अत: पशु पालक को प्रमुख बीमारियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है ताकि वह उचित समय पर उचित कदम उठा कर अपना आर्थिक हानि से बचाव तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा में भी सहयोग कर सके।दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग् निम्नलिखित है:
विषाणु जनित रोग :
(1) मुहं व खुर की बीमारी:
सूक्ष्म विषाणु (वायरस) से पैदा होने वाली बीमारी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है जैसेकि खरेडू,मुहं पका खुर पका, चपका,खुरपा आदि।यह बहुत तेज़ी फैलाने वाला छुतदार रोग है जोकि गाय, भैंस, भेड़, ब्क्रिम ऊंट, सुअर आदि पशुओं में हित है।विदेशी व संकर नस्ल रोग की गायों में यह बीमारी अधिक गम्भीर रूप से पायी जाती है। यह बीमारी हमारे देश में हर स्थान में होती है।इस रोग से ग्रस्त पशु ठीक होकर अत्यन्त कमज़ोर हो जाते हैं| दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है तथा बैल काफी समय तक कं करने योग्य नहीं रहते। शरीर पर बालों का कवर खुरदरा था खुर हरूप हो जाते हैं।
रोग का कारण:-मुंहपका-खुरपका रोग एक अत्यन्त सुक्ष्ण विषाणु जिसके अनेक प्रकार तथा उप-प्रकार है, से होता है।इनकी प्रमुख किस्मों में ओ,ए,सी,एशिया-1,एशिया-2,एशिया-3, सैट-1, सैट-3 तथा इनकी 14 उप-किस्में शामिल है।हमारे देश मे यह रोग मुख्यत: ओ,ए,सी तथा एशिया-1 प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। नम-वातावरण, पशु की आन्तरिक कमजोरी, पशुओं तथा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन तथा नजदीकी क्षेत्र में रोग का प्रकोप इस बीमारी को फैलाने में सहायक कारक हैं।
संक्रमण विधि:- यह रोग बीमार पशु के सीधे सम्पर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बिमार पशु की लार, मुंह, खुर व थनों में पड़े फफोलों में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा, तथा फर्श पर चार महीनों तक जीवित रह सकते हैं लेकिन गर्मीं के मौसम में यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं।विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ पशु के रक्त में पहुंचते हैं तथा लगभग 5 दिनों के अंदर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं।
रोग के लक्षण :- रोग ग्रस्त पशु को 104-106 डि. फारेनहायट तक बुखार हो जाता है। वह खाना-पीना व जुगाली करना बन्द कर देता है|दूध का उत्पादन गिर जाता है। मुंह से लार बहने लगती है तथा मुंह हिलाने पर चप-चप की आवाज़ आती हैं इसी कारण इसे चपका रोग भी कहते हैतेज़ बुखार के बाद पशु के मुंह के अंदर,गालों,जीभ,होंठ तालू व मसूड़ों के अंदर,खुरों के बीच तथा कभी-कभी थनों व आयन पर छाले पड़ जाते हैं| ये छाले फटने के बाद घाव का रूप ले लेते हैं जिससे पशु को बहुत दर्द होने लगता है। मुंह में घाव व दर्द के कारण पशु कहाँ-पीना बन्द कर देते हैं जिससे वह बहुत कमज़ोर हो जाता है।खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा चलने लगता है। गर्भवती मादा में कई बार गर्भपात भी हो जाता है।नवजात बच्छे-बच्छियां बिना किसी लक्षण दिखाए मर जाते है। लापरवाही होने पर पशु के खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं तथा कई बार खुरों के कवच भी निकल जाते हैं। हालांकि व्यस्क पशु में मृत्यु दर कम (लगभग 10%) है लेकिन इस रोग से पशु पालक को आर्थिक हानि बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। दूध देने वाले पशुओं में दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक हुए पशुओं का शरीर खुरदरा तथा उनमें कभी कभी हांफना रोग होजाता है। बैलों में भारी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती हैं ।
उपचार:- इस रोग का कोई निश्चित उपचार नहीं है लिकिन बीमारी की गम्भीरता को कम करने के लिए लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकैन्डरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह व खुरों के घावों को फिटकरी याँ पोटाश के पानी से धोते हैं।मुंह में बोरो-गिलिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है।
रोग से बचाव:-
(1) इस बीमारी से बचाव के लिए पशुओं को पोलीवेलेंट वेक्सीन के वर्ष में दो बार टीके अवश्य लगवाने चाहिए।बच्छे-बच्छियां में पहला टीका 1माह की आयु में, दूसरे तीसरे माह की आयु तथा तीसरा 6 माह की उम्र में और उसके बाद नियमित सारिणी के अनुसार टीके लगाए जाने चाहिए।
(2)बीमारी हो जाने पर रोग ग्रस्त पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए।
(3)बीमार पशुओं की देख-भाल करने वाले व्यक्ति को भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े से दूर रहना चाहिए।
(4)बीमार पशुओं के आवागमन पर रोक लगा देना चाहिए।
(5)रोग से प्रभावित क्षेत्र से पशु नहीं खरीदना चाहिए।
(6)पशुशाला को साफ-सुथरा रखना चाहिए।
(7)इस बीमारी से मरे पशु के शव को खुला न छोड़कर गाढ़ देना चाहिए।
2.पशु प्लेग (रिन्ड़रपेस्ट):
यह रोग भी एक विषाणु से पैदा वला छुतदार रोग है जोकि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। इनमें पशु को तीव्र दस्त अथवा पेचिस लग जाते हैं। यह रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके अतिरिक्त वर्तनों तथा देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा भी यह बीमारी फैल सकती है।इसमें पशु को तेज़ बुखार हो जाता है तथा पशु बेचैन हो जाता है। दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और पशु की आँखें सुर्ख लाल हो जाती है।2-3 दिन के बाद पशु के मुंह में होंठ, मसूड़े व जीभ के नीचे दाने निकल आटे हैं जो बाद में घाव का रूप ले लेते हैं।पशु में मुंह से लार निकलने लगती है तथा उसे पतले व बदबूदार दस्त लग जाते हैं जिनमें खून भी आने लगता है। इसमें पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है तथा उसमें पानी की कमी हो जाती है। इस बीमारी में पशु की 3-9 दिनों में मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी के प्रकोप से विश्व भर में लाखों की संख्या में पशु मरते ठे लेकिन अब विश्व स्ट् पर इस रोग के उन्मूलन की योजना के अंतर्गत भारत सरकार सरकार द्वारा लागू की गयी रिन्डरपेस्ट इरेडीकेशन परियोजना के तहत लगातार शत प्रतिशत रोग निरोधक टीकों के प्रयोग से अब यह बीमारी प्रदेश तथा देश में लगभग समाप्त हो चुकी है।
3.पशुओं में पागलपन या हलकजाने का रोग (रेबीज):
इस रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म विषाणु हलकाये कुत्ते, बिल्ली,बंदर, गीदड़, लोमड़ी या नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा नाडियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंच कर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। रोग ग्रस्त पशु की लार में यह विषाणु बहुतायत में होता है तथा रोगी पशु द्वारा दूसरे पशु को काट लेने से अथवा शरीर में पहले से मौजूद किसी घाव के ऊपर रोगी की लार लग जाने से यह बीमारी फैल सकती है। यह बीमारी रोग ग्रस्त पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकती है अत: इस बीमारी का जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। एक बार पशु अथवा मनुष्य में इस बीमारी के लक्षण पैदा होने के बाद उसका फिर कोई इलाज नहीं है तथा उसकी मृत्यु निश्चित है| विषाणु के शरीर में घाव आदि के माध्यम से प्रवेश करने के बाद 10दिन से 210 दिनों तक की अवधि में यह बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क के जितना अधिक नज़दीक घाव होता है उतनी ही जल्दी बीमारी के लक्षण पशु में पैदा हो जाते है जैसे कि सिर अथवा चेहरे पर काटे गए पशु में एक हफ्ते के बाद यह रोग पैदा हो सकता है।
लक्षण :- रेबीज़ मुख्यत: दो रूपों में देखी जाती है,पहला जिसमें रोग ग्रस्त पशु काफी भयानक हो जाता है तथा दूसरा जिसमें वह बिल्कुल शांत रहता है।पहले अथवा उग्र रूप में पशु में रोग के सभी लक्षण स्पष्ट दिखायी देते हैं लेकिन शांत रूप में रोग के लक्षण बहुत कम अथवा लहभ नहीं के बराबर ही होते हैं।
कुत्तों में इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था में व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तथा उनकी आंखे अधिक तेज नज़र आती हैं। कभी-कभी शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, 2-3 दिन के बाद उसकी बेचैनी बढ़ जाती है तथा उसमें बहुत ज्यादा चिड-चिडापन आ जाता है।वह काल्पनिक वस्तुओं की और अथवा बिना प्रयोजन के इधर-उधर काफी तेज़ी से दौड़ने लगता हैं तथा रास्ते में जो भी मिलता है उसे वह काट लेता हैं।अन्तिम अवस्था में पशु के गले में लकवा हो जाने के कारण उसकी आवा बदल जाती है, शरीर में कपकपी तथा छाल में लड़खड़ाहट आ जाती है तथा वह लकवा ग्रस्त होकर अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है।
गाय व भैंसों में इस बीमारी के भयानक रूप के लक्षण दिखते हैं।पशु काफी उत्तेजित अवस्था में दिखता है तथा वह बहुत तेजी से भागने की कोशिश करता हैं। वह ज़ोर-ज़ोर से रम्भाने लगता है तथा बीच-बीच में जम्भाइयाँ लेता हुआ दिखाई देता है। वह अपने सिर को किसी पेड़ अथवा दीवाल ले साथ टकराता है।कई पशुओं में मद के लक्षण भी दिखायी से सकते हैं। रोग ग्रस्त पशु ही दुर्बल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
मनुष्य में इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में उत्तेजित होना, पानी अथवा कोई खाद्य पदार्थ को निगलने में काफी तकलीफ महसूस करना तथा अंत में लकवा लकवा होना आदि है।
उपचार तथा रोकथाम:-एक बार लक्षण पैदा हो जाने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे ही किसी स्वस्थ पशु को इस बीमारी से ग्रस्त पशु काट लेता है उसे तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में ले जाकर इस बीमारी से बचाव का टीका लगवाना चाहिए। इस कार्य में ढील बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि ये टीके तब तक ही प्रभावकारी हो सकते हैं जब तक कि पशु में रोग के लक्षण पैदा नहीं होते।पालतू कुत्तों को इस बीमारी से बचने के लिए नियमित रूप से टीके लगवाने चाहिए तथा आवारा कुत्तों को समाप्त के देने चाहिए। पालतू कुत्तों का पंजीकरण सथानीय संस्थाओं द्वारा करवाना चाहिए तथा उनके नियमित टीकाकरण का दायित्व निष्ठापूर्वक मालिक को निभाना चाहिए।
(ख)जीवाणु जनित रोग
1.गलघोंटू रोग (एच.एस.):
गाय व भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक तथा छूतदार रोग है जुकी अधिकतर बरसात के मौसम में होता है यह गोपशुओं की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग नहुत तेज़ी से फैलकर बड़ी संख्या मे पशुओं को अपनी चपेट में लेकर उनकी मौर का कारण बन जाता हैं जिससे पशु पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज़ बुखार, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ निकालकर सांस लेना तथा सांस लेते समय तेज़ आवाज होया आदि शामिल है। कईं बार बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के ही पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है।
उपचार तथा रोकथाम:- इस रोग से ग्रस्त हुए पश को तुरन्त पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए अन्यथा पशु की मौत हो जाती है। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोग ग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगनिरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह की आयु में दूसरा 9 माह की अवस्था में तथा इसके बाद हर साल यह टीका लगाया जाता हैं। ये टीके पशु चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क लगाए जाते हैं।
2.लंगड़ा बुखार (ब्लैक क्कार्टर):
जीवाणुओं से फैलने वाला यह रोग गाय व भैंसों दोनों को होता है लिकिन गोपशुओं में यह बीमारी अधिक देखी जाती है तथा इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। इस रोग में पिछली अथवा अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाती हैं जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है या फिर बैठ जाता है। पशु को तेज़ बुखार हो जाता है तथा सूजन वाले स्थान को दबाने पर कड़-कड़ की आवाज़ आती है।
उपचार तथा रोकथाम:- रोग ग्रस्त पशु के उचार हेतू तुरन्त नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए ताकि पशु को शीघ्र उचित उपचार मिल सके, देर करने से पशु को बचना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा पैदा हुआ जहर (टोक्सीन) शरीर में पूरी को बचना लगभग असंभव हो जाता है जोकि पशु की मृत्यु का कारण बन जाता है। उपचार के लिए पशु को ऊँची डोज़ में प्रोकें पेनिसिलीन के टीके लगाए जाते हैं तथा सूजन वाले स्थान पर भी इसी दवा को सुई द्वारा माँस में डाला जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए पशु चिकित्सक संस्थाओं में रोग निरोधक टीके नि:शुल्क लगाए जाते है अत:पशु पालकों को इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाना चाहिए।
3.ब्रुसिल्लोसिस (पशुओं का छूतदार गर्भपात):
जीवाणु जनित इस रोग में गोपशुओं तथा भैंसों में गर्भवस्था के अन्तिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकाता है। मनुष्यों में यह उतार-चढ़ाव वाला बुखार (अज्युलेण्ट फीवर)नामक बीमारी पैदा करता है।पशुओं में गर्भपात से पहले योनि से अपारदर्शी पदार्थ निकलता है तथा गर्भपात के बाद पशु की जेर रुक जाती है। इसके अतिरिक्त यह जोड़ों में आर्थ्रायटिस (जोड़ों की सूजन) पैदा के सकता है।
उपचार व रोकथाम:- अब तक इस रोग का कोई प्रभावकरी उपचार नहीं हैं। यदि क्षेत्र में इस रोग के 5% से अधिक पशुओं को रोग हो तो रोग की रोकथाम के लिए बच्छियों में 3-6 माह की आयु में ब्रुसेल्ला-अबोर्टस स्ट्रेन-19 के टीके लगाए जा सकते हैं। पशुओं में प्रजनन की कृत्रिम गर्भाधान पद्धति अपना कर भी इस रोग से बचा जा सकता है।
(ग) रक्त प्रोटोज़ोआ जनित रोग-
1.बबेसिओसिस अथवा टिक फीवर (पशुओं के पेशाब में खून आना):
यह बीमारी पशुओं में एक कोशिकीय जीव जिसे प्रोटोज़ोआ कहते हैं से होती है। बबेसिया प्रजाति के प्रोटोज़ोआ पशुओं के रक्त में चिचडियों के माध्यम से प्रवेश के जाते हैं तथा वे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या बढ़ने लगते हैं जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कोशिकायें नष्ट होने लगती हैं। लाल रक्त किशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है जिससे पेशाब का रंग कॉफी के रंग का हो जाता है। कभी-कभी उसे खून वाले दस्त भी लग जाते हैं। इसमें पशु खून की कमी हो जाने से बहुत कमज़ोर हो जाता है पशु में पीलिया के लक्षण भी दिखायी देने लगते हैं तथा समय पर इलाज ना कराया जाय तो पशु की मृत्यु हो जाती है।
उपचार व रोकथाम:- यदि समय पर पशु का इलाज कराया जाये तो पहु को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। इसमें बिरेनिल के टीके पश के भर के अनुसार मांस में दिए जाते हैं तथा खून बढाने वाली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए उन्हें चिचडियों के प्त्कोप से बचना जरूरी है क्योंकि ये रोग चिचडियों के द्वारा ही पशुओं में फैलता है।
(घ)बाह्म तथा अंत: परजीवी जनित रोग-
1.पशुओं के शरीर पर जुएं,चिचडी तथा पिस्सुओं का प्रकोप:-
पशुओं के शरीर पर बाह्म परजीवी जैसे कि जुएं,पिस्सु या चिचडी आदि प्रकोप पर पशुओं का खून चूसते हैं जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है तथा वे कमज़ोर हो जाते हैं। इन पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता घट जाती है तथा वे अन्य बहुत सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बहुत से परजीवी जैसे कि चिचडियों आदि पशुओं में कुछ अन्य बीमारी जैसे टीक-फीवर का संक्रमण भी के देते हैं। पशुओं में बाह्म परजीवी के प्रकोप को रोकने के लिए अनेक दवाइयां उपलब्ध हैं जिन्हें पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार प्रयोग करके इनसे बचा जा सकता है।
2.पशुओं में अंत:परजीवी प्रकोप:-
पशुओं की पाचन नली में भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंत: परजीवी कहते हैं हैं। ये पशु के पेट, आंतों, यकृत उसके खून व खुराक पर निर्वाह करते हैं जिससे पहु कमज़ोर हो जाता है तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इससे पशु की उत्पादन क्षमता में भी कमी आ जाती है।
पशुओं को उचित आहार देने के बावजूद यदि वे कमजोर दिखायी दें तो इसके गोबर के नमूनों का पशु चिकित्सालय में परीक्षण करना चाहिए। परजीवी के अंडे गोबर के नमूनों में देखकर पशु को उचित दवा दी जाती है जिससे परजीवी नष्ट हो जाते हैं।
पशुओं के चारे का भंडारण :
पशुओं से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारे की आवश्यकता होती है। इन चारे को पशुपालक या तो स्वयं उगाता है या फिर खरीदता है। चारे की फसल उगने का एक खास समय होता है जोकि अलग-अलग चारे के लिए अलग-अलग है। चारे को अधिकांशत: हरी अवस्था में पशुओं को खिलाया जाता है तथा इसकी अतिरिक्त मात्रा को सुखाकर भविष्य में प्रयोग करने के लिए भंडार कर लिया जाता है ताकि चारे की कमी के समय उसका प्रयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सके।चारे का इस तरह से भंडारण करने से उसमें पोषक तत्व बहुत कम रह जाते है। इसी चारे का भंडारण यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाय तो उसकी पौष्टिकता में कोई कमी नहीं आती तथा कुछ खास त्रूकों से इस चारे को उपचारित करके रखने से उसकी पौष्टिकता को काफी हद तक बढाया भी जा सकता है। विभिन्न चारेको भंडारण करने की कुछ विधियाँ नीचे दी जा रही है।
1.घास को सुखाकर रखना (हे बनाना):
हे बनाने के लिए हरे कहरे या घास को इतना सुखाया जाता है जिससे कि उसके नमी कि मात्रा 15-20% तक ही रह जाय। इससे पादप कोशिकाओं तथा जीवाणुओं की एन्जाइम क्रिया रुक जाती है लेकिन इससे चारे की पौष्टिकता में कमी नहीं आती।हे बनाने के लिए लोबिया, बरसीम, लूसर्न, सोयाबीन, मटर आदि लेग्यूम्स तथा ज्वार, नेपियर, जौ, ज्वी, बाजरा, ज्वार, मक्की, गिन्नी, अंजन आदि घासों का प्रयोग किया जा सकता है। लेग्यूम्स घासों में सुपाच्य तत्व अधिक होते हैं तथा इसमें प्रोटीन व विटामिन ए.डी.व ई.भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए ये फसलें बहुत उपयुक्त होती है। हे बनाने के लिए चारा सुखाना हेतु निम्नलिखित तीन विधियों में से कोई भी विधि अपनायी जा सकती है।
(क) चारे को परतों में सुखाना:-जब चारे की फसल फूल आने वाली अवस्था में होती है तो उसे काटकर 9-9’की परतों में पूरे खेत में फैला देते हैं तथा बीच-बीच में उसे पलटते रकते हैं जब तक कि उसमें पानी की मात्रा लगभग 15% तक न रह जाय।इसके बाद इसे इकट्ठा कर लिया जाता है तथा ऐसे स्थान पर जहां वर्षा का पानी न आ सके इसका भंडारण कर लिया जाता है।
(ख) चारे को गट्ठर सुखाना:- इसमें चारे को काटकर 24 घण्टों तक खेत में पड़ा रहने देते हैं। इसके बाद इसे छोटी-छोटी ढेरियों अथवा गट्ठरों में बांध कर पूरे खेत में फैला देते हैं। इन गट्ठरों को बीच-बीच में पलटते रहते हैं जिससे नमी की मात्रा घट कर लगभग 18% तक हो जाए।
(ग) चारे को तिपाई विधि द्वारा सुखाना:-जहां भूमि अहिक गीली रहती हो अथवा जहां वर्षा अधिक होती हो ऐसे स्थानों पर खेतों में तिपाइयां गाढकर चारे की फसलों को उन पर फैला देते हैं।इस प्रकार वे भूमि के बिना संपर्क में आए हवा व धुप से सूख जाती है। कई स्थानों पर घरों की क्षत पर भी घासों को सुखा कर हे बनाया जाता है। प्रदेश मे मध्यम व ऊंचे क्षेत्रों में हे (सूखे घास) को कूप अथवा गुम्बद की शक्ल के ढेर जिन्हें स्थानीय भाषा में घोड़ कहते हैं में ठीक ढंग से व्यवस्थित करके रखा जाता है। इनका आकार कोन की तरह होने के कारण इन पर वर्षा का पानी खड़ा नहीं हो पाता जिससे चारे की पौष्टिकता में कमी नहीं आती।
2.सूखे चारे की पौष्टिकता बढ़ाना :
(चारे का यूरिया द्वारा उपचार) सूखे चारे जैसे भूसा (तूड़ी), पुराल आदि में पौष्टिक तत्व लिगनिन के अंदर जकड़े रहते हैं जोकि पशु के पाचन तन्त्र द्वारा नहीं किए जा सकते। इन चरों का कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा उपचार करने इनके पोषक तत्वों को लिगनिन से अलग कर लिया जाता है। इसके लिए यूरिया उपचार की विधि सबसे सस्ती तथा उत्तम है।
उपचार की विधि : एक क्विंटल सूखे चारे जैसे पुआल या तूड़ी के लिए चार किलो यूरिया का 50 किलो साफ पानी में घोल बनाते है । चारे को समतल तथा कम ऊंचाई वाले स्थान पर 3-4 मीटर की गोलाई में 6″ ऊंचाई की तह में फैला कर उस पर यूरिया के घोल का छिड़काव करते हैं। चारे को पैरों से अच्छी तरह दबा कर उस पर पुन: सूखे चारे की एक और पर्त बिछा दी जाती है और उस पर यूरिया के घोल का समान रूप से छिड़काव किया जाता है , 25 क्विंटल की ढेरी बनाकर उसे एक पोलीथीन की शीट से अच्छी तरह सेध्क दिया जाता है।यदि पोलीथीन की शीट उपलब्ध न हो तो उपचारित चारे की ढेरी को गुम्बदनुमा बनाते हैं जिसे ऊपर से पुआल आदि से ढक दिया जाता है। उपचारित चारे को 3 सप्ताह तक ऐसे ही रखा जाता है जिससे उसमें अमोनिया गैस बनती है जो घटिया चारे जो पौष्टिक तथा पाच्य बना देती है। इसके बाद इस चारे को पशु को खालिस या फिर हरे चारे के साथ मिलाकर खिलाया जा सकता है।
(यूरिया उपचार से लाभ )
(1) उपचारित चारा नरम व स्वादिष्ट कोने के कारण पशु उसे खूब चाव से खाते हैं तथा चारा बर्बाद नहीं होता।
(2) पांच या 6 किलों उपचारित पुआल खिलने से दुधारू पशुओं में लगभग 1 किलो दूध की वृद्धि हो सकती है।
(3) यूरिया उपचारित चारे को पशु आहार में सम्मिलित करने से दाने में कमी की जा सकती है जिससे दूध के उत्पादन की लागत कम हो सकती है।
(4) बछड़े-बच्छियों को यूरिया उपचारित चारा खिलाने से उनका बजन तेज़ी से बढता है तथा वे स्वस्थ दिखायी देते है।
सावधानियाँ:-
(1) यूरिया का घोल साफ पानी में तथा यूरिया की सही मात्रा के साथ बनाना चाहिए।
(2) घोल में यूरिया पूरी तरह से घुल जानी चाहिए।
(3) उपचारित चारे को 3 सप्ताह से पहले पशु को कदापि नहीं खिलाना चाहिए।
(4) यूरिया के घोल को चारे के ऊपर समान रूप से छिड़काव चाहिए।
3.साइलेज बनाना:-
हरा चारा जिसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है को हवा की अनुपस्थिति में जब किसी गड्ढे में दबाया जाता है तो किण्डवन की क्रिया से वह चारा कुछ समय बाद एक अचार की तरह बन जाता है जिसे साइलेज कहते हैं।हरा चारा की कमी होने पर साइलेज का प्रयोग पशुओं को खिलने के लिए किया जाता है।
साइलेज बनाने योग्य फसलें:-
साइलेज लगभग सभी घासों से अकेले अथवा उनके मिश्रण से बनाया जा सकता है। जीन फसलों में घुलनशील कार्बोहाईड्रेट्स अधिक मात्रा में होते हैं जैसे कि ज्वार,मक्की, जवी, गिन्नी घास, नेपियर, सिटीरिया तथा घास्नियों की घास आदि,साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त होती हैं। फलीदार जिनमें कार्बोहाइड्रेटस कम तथा नमी की मात्रा अधिक होती हैं, को अधिक कार्बोहाइड्रेटस वाली फसलों के साथ मिलाकर अथवा शीरा मिला कर साइलेज के लिए प्रयोग जा सकता है। साइलेज बनाने के लिए चारे की फसलों को फूलने से लेकर दानों के दूधिया होने तक की अवस्था में काट लेना चाहिए।साइलेज बनाते समय चारे में नमी की मात्रा 65% होनी चाहिए।
साइलेज के गड्ढे/साइलोपिट्स:-
साइलेज जीन गड्ढों मरण बनाया जाता है उन्हें साइलोपिट्स कहते हैं। साइलोपिट्स कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे ट्रेन्च साइलो बनाने सस्ते व आसान होते हैं।आठ फुट व्यास तथा 12 फुट गहराई वाले गड्ढे में 4 पशुओं के लिए तीन माह तक का साइलेज बनाया जा सकता है। गड्ढा (साइलो)ऊंचा होना चाहिए तथा इसे भली प्रकार से कूटकर सख्त बना लेना चाहिए। साइलो के फर्श व दीवारें पक्की बनानी चाहिए और यदि ये संभव न हो तो दीवारों की लिपाई भी की जा सकती है।
साइलेज बनाने की विधि:-
साइलेज बनाने के लिए जिस भी हरे चारे का इस्तेमाल करना हो, उसे उपयुक्त अवस्था में खेत से काट कर 2 से 5 सेन्टीमीटर के टुकड़ों में कुट्टी बना लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चारा साइलो पिट में दबा कर भरा जा सके। कुट्टी किया हुआ चारा खूब दबा-दबा कर रखें जाते हैं ताकि बरसात का पानी ऊपर न टिक सके। फिर इसके ऊपर पोलीथीन की शीट बिछाकर ऊपर से 18-20 से.मी. मोटी मिट्टी की पर्त बिछा दी जाती है। इस परत को गोबर व चिकनी मिट्टी से लीप दिया जाता है। दरारें पड़ जाने पर उन्हें मिट्टी से बन्द करते रहना चाहिए ताकि हवा व पानी गड्ढे में प्रवेश न कर सकें। लगभग 45 से 60 दिनों में साइलेज बन कर तैयार हो जाता है जिसे गड्ढे को एक तरफ से खोलकर मिट्टी व पोलोथीन शीट हटाकर आवश्यकतानुसार पशु को खिलाया जा सकता है। साइलेज निकालकर गधे को पुन: पोलीथीन शीट व मिट्टी से ढक देना चाहिए। प्रारम्भ में साइलेज को थोड़ी मात्रा में अन्य चारों के साथ मिला कर पशु को खिलाना चाहिए तथा धीरे-धीरे पशुओं को इसका स्वाद लग जाने पर इसकी मात्रा 20-30 किलो ग्राम प्रति पशु तक बढायी जा सकती है।कृप्या आप इस लेख को भी पढ़ें हिंदी पशुपालन गाइड-भाग १
